- डॉ अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)
हाल ही में देश ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। परेड, सांस्कृतिक झांकियाँ, राष्ट्रपति का संबोधन और राष्ट्रगान की गूंज, ये सभी दृश्य एक बार फिर हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बने। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी ने हमें गर्व का अनुभव कराया, लेकिन गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं होता। यह वह अवसर होता है जब एक राष्ट्र स्वयं से अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने नागरिक व्यवहार के बारे में संवाद करता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान केवल सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज़ नहीं था। वह स्वतंत्र भारत का नैतिक घोषणापत्र था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि आज़ादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना है जहाँ नागरिक और राज्य के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलित संबंध हो।
भारतीय संविधान को प्रायः ‘अधिकारों का दस्तावेज़’ कहा जाता है, और यह कथन गलत भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और गरिमा का अधिकार, इन मौलिक अधिकारों ने भारतीय नागरिकों को वह सुरक्षा और आत्मविश्वास दिया, जो औपनिवेशिक काल में कल्पना से परे था। पहली बार राज्य नागरिक की गरिमा का संरक्षक बना, न कि उसका स्वामी। लेकिन संविधान की आत्मा केवल अधिकारों में नहीं, बल्कि उस संतुलन में निहित है जो वह अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच स्थापित करता है।
संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि यदि स्वतंत्रता को उत्तरदायित्व से अलग कर दिया गया, तो लोकतंत्र दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसी सोच के परिणामस्वरूप संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को स्थान मिला। यह केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक गहरा नैतिक संदेश था कि लोकतंत्र केवल मांगों से नहीं, सहभागिता से चलता है। नागरिक जितने अधिकारों के प्रति सजग हों, उतने ही कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होना आवश्यक है।
लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा चुनावी परिणामों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के सार्वजनिक जीवन में होती है। जब कानून हमारे पक्ष में न हो, तब भी क्या हम उसका सम्मान करते हैं, यही पहली कसौटी है। जब हमारे विचारों से भिन्न मत सामने आते हैं, तब क्या हम संवाद का मार्ग चुनते हैं या अपमान और बहिष्कार का रास्ता चुनते हैं, यही दूसरी कसौटी है। और जब हमारे पास संख्या, प्रभाव या सत्ता होती है, तब क्या हम संयम बरतते हैं या उसे थोपने का प्रयास करते हैं! यही लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा है।
संविधान ने हमें अधिकार इसलिए नहीं दिए कि हम दूसरों को चुप करा सकें, बल्कि इसलिए दिए कि हम स्वयं बिना भय के बोल सकें। उसने हमें स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी कि हम नियमहीन हो जाएँ, बल्कि इसलिए दी कि हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन का अंत नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन की शुरुआत है। यही अंतर संविधान हमें लगातार याद दिलाता है।
वर्तमान समय में अधिकारों की भाषा अत्यंत मुखर हो गई है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि अधिकारों के बिना कोई भी समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जब अधिकार ज़िम्मेदारी से कट जाते हैं, तब वे संवाद के बजाय टकराव का माध्यम बन जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि संवेदनशीलता से रहित हो जाए, तो वह समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करती है। विरोध का अधिकार यदि व्यवस्था को नष्ट करने का औज़ार बन जाए, तो वह लोकतंत्र को मज़बूत नहीं, कमज़ोर करता है।
कर्तव्य की अवधारणा अक्सर अधिकारों के शोर में दब जाती है, जबकि वास्तव में वही लोकतंत्र की नींव है। मतदान करना, कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये केवल संवैधानिक शब्द नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन की अनिवार्य शर्तें हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं, तब राज्य को कठोर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब नागरिक अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं, तब सबसे अच्छे कानून भी निष्प्रभावी हो जाते हैं।
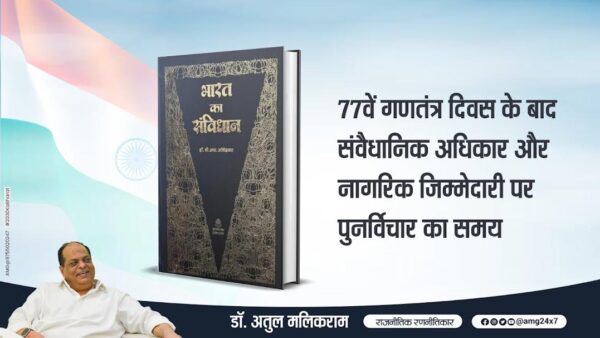














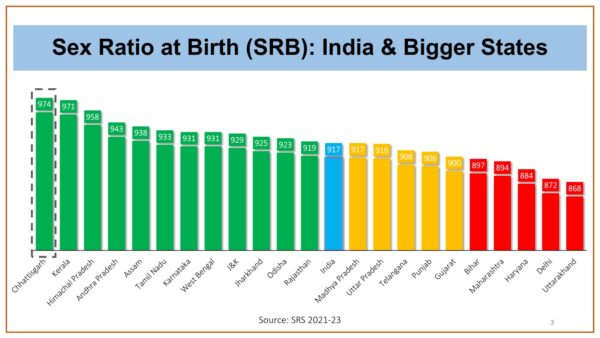
Leave a Reply